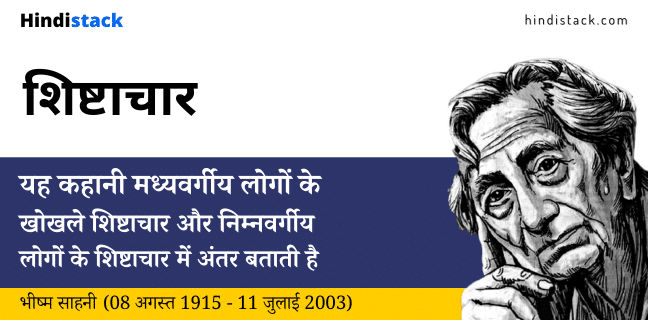चाहिए तो यह था कि मेरी पहली कहानी प्रेम-कहानी होती। उम्र के एतबार से भी यही मुनासिब था और अदब के एतबार से भी। पर प्रेम के लिए (और प्रेम कहानी के लिए भी) अनुकूल परिस्थितियाँ हों तब काम बने। मैंने वही लिखा जो मेरे जैसे माहौल में पहले वाले सभी भारतीय युवक लिखते हैं- अबला नारी की कहानी। हिंदी के अधिकांश लेखकों का तो साहित्य में पदार्पण अबला नारी की कहानी से ही होता है और यह दुखांत होनी चाहिए। मैंने भी वैसे ही किया है। बड़ी बेमतलब, बेतुकी कहानी थी, न सिर, न पैर और शुरू से आखिर तक मनगढ़ंत, पर चूँकि अबला नारी के बारे में थी और दुखांत थी, इसलिए वानप्रस्थी जी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता था, और पिताजी को भी नहीं, इसलिए कहानी, कालिज पत्रिका में स्थान पा गई।
पर इसके कुछ ही देर बाद एक प्रेमकहानी सचमुच कलम पर आ ही गई। नख-शिख से प्रेम-कहानी ही थी, पर किसी दूसरी दुनिया की कहानी, जिससे मैं परिचित नहीं था। तब मैं कालिज छोड़ चुका था, और पिताजी के व्यापार में हाथ बँटाने लगा था। कालिज के दिन पीछे छूटते जा रहे थे, और आगे की दुनिया बड़ी ऊटपटाँग और बेतुकी-सी नज़र आ रही थी। हर दूसरे दिन कोई-न-कोई अनूठा अनुभव होता। कभी अपने घुटने छिल जाते, कभी किसी दूसरे को तिरस्कृत होते देखता। मन उचट-उचट जाता। तभी एक दिन बाज़ार में… मुझे दो प्रेमी नज़र आए।
शाम के वक्त, नमूनों का पुलिंदा बगल में दबाए मैं सदर बाज़ार से शहर की ओर लौट रहा था, जब सरकारी अस्पताल के सामने, बड़े-से नीम के पेड़ के पास मुझे भीड़ खड़ी नज़र आई। भीड़ देखकर मैं यों भी उतावला हो जाया करता था, कदम बढाता पास जा पहुँचा। अंदर झाँककर देखा तो वहाँ दो प्रेमियों का तमाशा चल रहा था। टिप्पणियाँ और ठिठोली भी चल रही थी। घेरे के अंदर एक युवती खड़ी रो रही थी और कुछ दूरी पर एक युवक ज़मीन पर बैठा, दोनों हाथों में अपना सिर थामे, बार-बार लड़की से कह रहा था, ” राजो, दो दिन और माँग खा। मैं दो दिन में तंदुरुस्त हो जाऊँगा। फिर मैं मजूरी करने लायक हो जाऊँगा।” और लड़की बराबर रोए जा रही थी। उसकी नीली-नीली आँखें रो-रोकर सूज रही थीं। “मैं कहाँ से माँगूँ ? मुझे अकेले में डर लगता है।” दोनों प्रेमी, आस – पास खड़ी भीड़ को अपना साक्षी बना रहे थे। “देखो बाबूजी, मैं बीमार हूँ। इधर अस्पताल में पड़ा हूँ। मैं कहता हूँ दो दिन और माँग खा, फिर मैं चंगा हो जाऊँगा।” लड़की लोगों को अपना साक्षी बनाकर कहती, “यहाँ आकर बीमार पड़ गया, बाबूजी मैं क्या करूँ ? इधर पुल पर मजूरी करती रही हूँ, पर यहाँ मुझे डर लगता है।”
पता चला कि दोनों प्रेमी गाँव से भागकर शहर में आए हैं, किसी फकीर ने उनका निकाह भी करा दिया है, फटेहाल गरीबी के स्तर पर घिसटने वाले प्रेमी! शहर पहुँचकर कुछ दिन तक तो लड़के को मज़दूरी मिलती रही। पास ही में एक पूल था। वह पूल के एक छोर से सामान उठाता और दूसरे छोर तक ले जाता, जिस काम के लिए उसे इकन्नी मिलती। कभी किसी की साइकिल तो कभी किसी का गठ्टर। हनीमून पूरे पाँच दिन तक चला। दोनों ने न केवल खाया पिया, बल्कि लड़के ने अपनी कमाई में से जापानी छींट का एक जोड़ा भी लड़की को बनवा कर दिया, जो उन दिनों अढ़ाई आने गज़ में बिका करती थी।
इस पर लड़का तड़पकर कहता, “देख राजो, मुझे छोड़कर नहीं जा। इसे समझाओ बाबूजी, यह मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इसे मैं कहाँ ढूँढूँगा।” “यहाँ मुझे डर लगता है। मैं रात को अकेली सड़क पर कैसे रहूँ ?”
दोनों रो रहे थे और तमाशबीन खड़े हँस रहे थे। कोई लड़की की नीली आँखों पर टिप्पणी करता, कोई उनके ‘ऐसे-वैसे’ प्रेम पर, और सड़क की भीड़ में खड़े लोग केवल आवाज़ें ही नहीं कसते, वे इरादे भी रखते हैं। और एक मौलवीजी लड़की की पीठ सहलाने लगे थे और उसे आश्रय देने का आश्वासन देने लगे थे। और प्रेमी बिलख- बिलख कर प्रेमिका से अपने प्रेम के वास्ते डाल रहा था।
तभी, पटाक्षेप की भाँति अँधेरा उतरने लगा था और पीछे अस्पताल की घण्टी बज उठी थी जिसमें प्रेमी युवक भरती हुआ था, और वह गिड़गिड़ाता, चिल्लाता, हाथ बाँधता, लड़की से दो दिन और माँग खाने का प्रेमालाप करता अस्पताल की ओर सरकने लगा और मौलवीजी सरकते हुए लड़की के पास आने लगे, और घबराई, किंकर्त्तव्यविमूढ़ लड़की, मृग शावक की भाँति सिर से पैर तक काँप रही थी… नायक भी था, नायिका भी थी, खलनायक भी था, भाव भी था, विरह भी और कहानी का अंत अनिश्चय के धुँधलके में खोया हुआ भी था।
मैं यह प्रेम कहानी लिखने का लोभ स्ंवरण नहीं कर सका। लुक छिपकर लिख ही डाली, जो कुछ मुद्दत बाद ‘नीली आँखें’ शीर्षक से, अमृतरायजी के सम्पादकत्व में हंस में छपी, इसका मैंने आठ रुपये मुआवज़ा भी वसूल किया जो आज के आठ सौ रुपये से भी अधिक था।